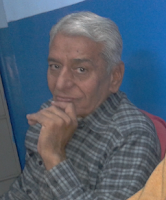भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंह ने पार्टी के तमाम नेताओं-कार्यकर्ताओं को हड़का दिया है - ‘चुप रहो! नरेन्द्र मोदी को प्रधान मन्त्री बनाने का हल्ला-गुल्ला बन्द करो।’ असर हुआ तो जरूर किन्तु सौ टका नहीं। गुबार बैठा तो सही किन्तु गर्द अभी भी बनी हुई है। शोर थमा तो जरूर किन्तु धीमी-धीमी भिनभिनाहट हवाओं में गूँज रही है। कुछ बिगड़ैल बच्चे हर कक्षा में होते हैं जो अपने-अपने मास्टरजी की नाक में दम किए रहते हैं। देखिए न! राहुल ने सरे आम हड़काया लेकिन बेनी बाबू ने सुना?
इस बीच, अभी-अभी ही, एक बात और हो गई। वेंकैया नायडू ने कह दिया कि पार्टी की ओर से किसे प्रधान मन्त्री घोषित किया जाए - यह फैसला, भाजपा का संसदीय बोर्ड तय करेगा। नायडू का कहना याने पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य! गोया नायडू ने, वायुमण्डल में ठहरी हुई, थेड़ी-बहुत गर्द पर पानी की बौछार कर दी और हवाओं में बनी हुई भिनभिनाहट को म्यूट कर दिया।
ऐसे में अब, जबकि नरेन्द्र मोदी के प्रधान मन्त्री की दावेदारी को लेकर पार्टी, आसमान को साफ और हवाओं को निःशब्द कर चुकी हो, जब मैं खुद ही कह चुका हूँ कि मोदी के प्रधान मन्त्री न बनने का तीसरा कारण ‘सुपरिचित, जगजाहिर और घिसा-पिटा’ है, तो इस तीसरी कड़ी की क्या आवश्यकता और औचित्य?
मुझे किसी की भी सामान्य-समझ (कॉमनसेन्स), दूरदर्शिता और चीजों को समझने की क्षमता पर रंच मात्र भी सन्देह नहीं। लेकिन मैंने अपनी ओर से वादा किया था। सो, उसे ही निभाने के लिए यह तीसरी कड़ी।
तर्क और अनुमान तो, अपनी सुविधा और इच्छानुसार जुटाए और गढ़े जा सकते हैं किन्तु गणित में यह सुविधा नहीं मिल पाती। तर्क शास्त्र का सहारा लेकर, दो और दो को पाँच साबित करने का चमत्कार दिखानेवाले जादूगर को भी, किराने की दुकान पर पाँचवा रुपया नगद गिनवाकर चुकाने पर ही पाँच रुपयों की कीमत का सौदा-सुल्फ मिल पाता है। तर्कों की अपनी हकीकत हो सकती है किन्तु हकीकतों के कोई तर्क नहीं हो पाते। यह ‘तर्क रहित हकीकत’ ही नरेन्द्र मोदी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है।
यहाँ फिर एक बार मालवी की एक कहावत मेरी बात को आसान करती है। यह मालवी कहावत है - ‘ओछी पूँजी घर धणी ने खाय।’ अर्थात्, कम पूँजी के दम पर व्यापार नहीं किया जा सकता। कम पूँजी पर व्यापार करनेवाला व्यापारी अन्ततः डूबता ही डूबता है। डूबने से बचने का एक ही उपाय है - प्रचुर पूँजी। यदि प्रचुर न हो तो उसका यथेष्ट (जरूरत के मुताबिक) होना तो अनिवार्य है ही। अपनी पूँजी कम हो और खुद को बचाए रखने की ललक हो तो अपने जैसे, कम पूँजीवाले किसी दूसरे व्यापारी को तलाशा जाता है। तब, कम पूँजीवाले दो व्यापारियों की सकल पूँजी मिलकर जरूरत के मुताबिक हो जाती है। दोनों के मिलने के बाद भी पूँजी कम पड़े तो, कम पूँजीवाले किसी तीसरे की तलाश की जाती है। आवश्यकतानुसार यह सिलसिला बढ़ता चला जाता है और तब ही थमता है जब कि कम पूँजीवाले ऐसे तमाम व्यापारी खुद को बचाए रखने की स्थिति में आ जाएँ। व्यापार में ऐसे उपक्रम को भागीदारी या प्रायवेट लिमिटेड कहा जाता है जबकि राजनीति में इसे ‘गठबन्धन’ कहा जाता है। राजग (एनडीए) और संप्रग (यूपीए), भारतीय राजनीति के, ओछी पूँजीवाले ऐसे ही व्यापारियों के जमावड़े हैं जहाँ खुद को बचाए रखने के लिए साथवाले को बचाए रखना ‘विवशताजनित बुद्धिमानी और व्यवहारिकता’ बरती जा रही है। दिलजले लोग इसे इसे, ‘मीठा खाने के लिए जूठन खाना’ कहते हैं।
अब यह कहनेवाली बात नहीं रही कि दिल्ली में अपने दम पर सरकार बना पाना न तो काँग्रेस के लिए सम्भव है और न ही भाजपा के लिए। दोनों को बैसाखियाँ चाहिए ही चाहिए। मजे की बात है कि सारी की सारी ‘बैसाखियाँ’ इन दोनों दलों पर बिलकुल ही भरोसा नहीं करतीं। भरोसा करना तो बाद की बात रही, सबकी सब इन दोनों से भयाक्रान्त बनी रहती हैं। कभी-कभी तो यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये ‘बैसाखियाँ’ किस कारण इन्हें सहारा देती हैं - सत्ता में भागीदारी के लाभ लेने के लिए या येन-केन-प्रकारेण अपना अस्तित्व बचाए और बनाए रखने के लिए? अपने लिए इन्हें इन दोनों में से किसी न किसी के साथ जुड़ना ही पड़ता है। सो, ये सब, ‘कम हानिकारक’ को चुनती रहती हैं। करुणा (निधि), ममता, माया और जय ललिता, के पास ‘दोनों घाटों पर सत्ता-स्नान के अनुभव की अतिरिक्त/विशेष योग्यता’ है। कुछ दल ऐसे हैं जिन्हें या तो भाजपा के ही साथ रहना है या फिर काँग्रेस के साथ ही। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पहचान ‘काँग्रेस विरोध’ है और जो शुरु से हैं तो राजग (एनडीए) के साथ किन्तु पाला बदलने में उन्हें रंच मात्र भी असुविधा नहीं होगी और क्षण भर की देरी नहीं लगेगी। जनता दल युनाइटेड (जदयू) और बीजू जनता दल (बीजद), राजग के ऐसे ही दो साथी हैं। इनका जो आयतन और घनत्व राजग के लिए ‘अपरिहार्य होने की सीमा तक महत्वपूर्ण’ है, इनका वही आयतन और घनत्व, भाजपा के लिए चिन्ता और मुश्किलें बढ़ाता है। उड़ीसा में नवीन बाबू (बीजद) ने भाजपा की बोलती ही बन्द कर रखी है जबकि बिहार में नीतिश की मुस्कान ‘जानलेवा’ बनी हुई है। राजग के घटकों की कम होती संख्या, इन दोनों दलों की अपरिहार्यता और महत्व में बढ़ोतरी ही करती है।
हालाँकि यह कल्पना में भी सम्भव नहीं है किन्तु राजनीतिक आकलन में मूर्खतापूर्ण दुस्साहस बरतते हुए कल्पना की जा सकती है कि बाकी सारे घटक भले ही एक बार, नरेन्द्र मोदी के नाम पर ‘मूक सहमति’ जता दें किन्तु उड़ीसा और बिहार के दोनों जननायक ऐसा कभी नहीं करेंगे। करते तो भला ऐसी, सतही और कच्ची विचार-भूमिवाली आलेख-श्रृंखला की गुंजाइश बन पाती?
यही भाजपा का संकट है और मोदी के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा भी। अकाली दल जैसे घटकों को छोड़ दें तो बाकी सारे घटकों का काम, भाजपा के बिना चल सकता है किन्तु इन सबके बिना भाजपा का काम नहीं चल सकता। सत्ता की व्यसनी काँग्रेस के लिए नवीन पटनायक और नीतिश को कबूल करना तनिक भी कठिन नहीं होगा। समाजवादी विचारधारा के सूत्र काँग्रेस से जुड़ने में कोई मानसिक बाधा नहीं होगी। धर्मनिरपेक्षता की रक्षा और साम्प्रदायिकता के विरोध के नाम पर तो बिलकुल ही नहीं। सामान्य समझ रखनेवाला राजनीतिक प्रेक्षक भी जानता है कि नवीन पटनायक और नीतिश को लपकने के लिए काँग्रेस आतुर बैठी है जबकि मोदी को प्रधानमन्त्री बनाने के नाम पर इन्हें राजग में बनाए रखना, भाजपा के लिए असम्भवप्रायः ही है। ऐसे में, यह कहना अधिक ठीक होगा कि इन दोनों को साथ बनाए रखना नहीं बल्कि इन दोनों के साथ बने रहना भाजपा की अपरिहार्यता भी है और मजबूरी भी।
इसी बीच, राजग के संयोजक और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव की, अभी-अभी छोड़ी गई, एक ‘छछूँदर’ ने यदि भाजपा की नींद उड़ा दी हो तो अचरज नहीं। शरद यादव ने, राजग के घटकों में बढ़ोतरी की कोशिशें करने की आवश्यकता जताई है। इस 'छछूँदर' का राजनीतिक पेंच यह कि जितने अधिक घटक दल होंगे, भाजपा को उतने अधिक दलों की खुशामद करनी पडेगी। घटक दलों की अधिकता, भाजपा का वजन भी कम करेगी। अटलजी के बाद भाजपा में ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जिसके नाम पर, राजग के सारे घटक सहमत हो जाएँ। यह अटलजी का ही करिश्मा था कि लगभग सवा दो दर्जन दल, राजग में प्रेमपूर्वक बने हुए थे। आज तो स्थिति यह हो गई है कि गिनती के घटकों को सम्हाले रखना भाजपा के लिए सर्कसी-करतब से कम कठिन नहीं हो रहा है। ऐसे में मोदी के नाम का असर इन सब पर बिलकुल वैसा ही होता नजर आ रहा है मानो कनखजूरे पर शकर डाली जा रही हो।
मौजूदा राजग : ढेर सारे चले गए, गिनती के रह गए
ऐसे में, जबकि 2014 के चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलना नहीं है, जबकि बाकी सबका काम भाजपा के बिना चलता नजर आ रहा हो लेकिन इनके बिना भाजपा का काम चलना नहीं, जबकि काँग्रेस ने सबके लिए सारे रास्ते खुले रखे हुए हों लेकिन मोदी के नाम पर भाजपा के सारे रास्ते बन्द होते नजर आ रहे हों और सत्ता का मीठा खाने के लिए उसे जब सहयोगी दलों पर ही निर्भर होना है तो उसे ‘राग मोदी’ आलापना बन्द करना ही पड़ेगा। ऐसा वह कर भी लेगी। सत्ता जरूरी है, मोदी नहीं। सत्ता के लिए जब ‘राष्ट्रीय अस्मिता’ और ‘धार्मिक आस्था’ के अपने (राम मन्दिर, समान नागरिक संहिता और धारा 370 जैसे) तमाम ‘बेस्ट सेलेबल मुद्दे’ हिन्द महासागर में डुबाए जा सकते हों (याद करें कि राजग गठन के समय केवल भाजपा ने अपने मुद्दे छोड़े थे, अन्य किसी भी दल ने अपना कोई मुद्दा नहीं छोड़ा था) तो ‘एक आदमी’ से जान छुड़ाना तो बिलकुल ही मुश्किल नहीं होगा। फिर, मोदी के बहाने एक बार फिर वही पुरानी (भाजपा और संघ की, एक साथ दोहरी सदस्यतावाली) बहस शुरु होने की आशंका बलवती हो जाएगी जिसके चलते जनता पार्टी का विघटन हुआ था! भाजपा इस वक्त तो यह जोखिम बिलकुल ही नहीं लेना चाहेगी।
इसलिए, जबकि खाँटी संघी और नादान भाजपाई भी मान रहे हों कि 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलना नहीं (कोई भी 160-180 से आगे नहीं बढ़ रहा) और सहयोगी दलों की ‘अनुकम्पा’ के बिना दिल्ली दूर ही रहनी है तो फिर वही किया जाएगा जो करना पड़ेगा - मोदी के नाम से इस तरह मुक्ति पाई जाएगी जैसे कि कोई भी ‘समझदार’ आदमी, खटमलों भरी रजाई से पाता है - उसे फेंक कर। सो, बहुमत का नौ मन तेल नहीं मिलेगा और इसीलिए प्रधानमन्त्री पद पर, राधा के नाच की तरह मोदी नजर नहीं ही आएँगे।
लेकिन, राधा का और नाच का कोई न कोई रिश्ता है तो जरूर! नहीं होता तो भला यह कहावत कैसे बनती? तो ‘नाच’ के नाते से जुड़ी यह राधा यदि नाचेगी नहीं तो ठुमकेगी भी नहीं? इसके पाँव भी नहीं उठेंगे? क्या करेगी यह राधा?
बेबात की इसी बात में बात तलाश करने की कोशिश, अगली, ‘चकल्लसी’ कड़ी में।