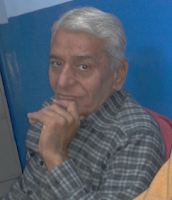वे बरसों तक, मन्दसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के एक समृद्ध गाँव के ‘पटेल’ बने रहे। वे उस जमाने के ‘इण्टर पास’ हैं जिस जमाने में मेट्रिक पास होना ही किसी को दर्शनीय बना देता था। अच्छी-खासी सरकारी नौकरी मिल रही थी लेकिन न तो ताबेदारी (अधीनस्थता) कबूल न ही बँध कर रहना। सो इंकार कर दिया। परिवार के पास सिंचित जमीन का भरपूर रकबा। खुद को खेती में झोंक दिया। ‘इण्टर पास पेण्टधारी जण्टरमेन’ को खेतों में बुवाई, सिंचाई, निंदाई-गुड़ाई करते देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते।
आज तो नीमच अलग जिला है लेकिन तब वह मन्दसौर जिले का उप सम्भाग (सब डिविजन) हुआ करता था। प्रदेश को, सुन्दरलालजी पटवा और वीरेन्द्रकुमारजी सकलेचा जैसे दो-दो मुख्यमन्त्री देने की पहचान से पहले मन्दसौर जिले की पहचान अफीम के लिए रही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम मन्दसौर जिले में ही पैदा होती है। अफीम की खेती वहाँ आज भी एक महत्वपूर्ण ‘सामाजिक प्रतिष्ठा-प्रतीक’ है। आज तो स्थिति लगभग आमूलचूल बदल गई है किन्तु तब माना जाता था कि प्रत्येक अफीम उत्पादक किसान किसी न किसी स्तर पर अफीम तस्करी से जुड़ा हुआ है।
जैसा कि ‘पटेल बा’ ने बताया, उनका गाँव अफीम उत्पादक गाँवों मे अग्रणी था। नामचीन अफीम तस्कर और उनके कारिन्दे इस गाँव मे अक्सर नजर आते थे। एक बार अफीम का बड़ा सौदा हुआ। गाँव के कई किसान इस सौदे में शरीक थे। पढ़े-लिखे और प्रतिभाशाली होने के कारण पटेल बा को गाँव की ओर से प्रभारी बनाया गया। तय हुआ कि फलाँ तारीख की रात को तस्कर के लोग आकर अफीम की डिलीवरी लेंगे। भागीदार किसानों की अफीम पटेल बा के घर में इकट्ठी की गई।
एक तो बड़ा सौदा और दूसरे, माथे पर जिम्मेदारी। सो, पटेल बा ने अपने पक्के मकान की छत पर खाट बिछाई। अमावस की रात। माहौल में अफीम की मादक गन्ध। लेकिन पटेल बा की आँखों ने नींद को अनुमति नहीं दी। कभी खाट पर बैठें तो कभी छत पर चहल कदमी करें।
आधी रात होने को आई। तस्कर के कारिन्दों के आने का समय हो चला था। पटेल बा की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। ऐसा काम अब तक छुटपुट स्तर पर ही किया था। इतने बड़े स्तर का पहला मौका था। उनकी आँखें मानो मशालें बन जाना चाह रही थीं। अँधेरे को घूर कर और चीर कर दूर-दूर तक देखने, टोह लेने की कोशिशें जारी थीं।
लेकिन पटेल बा चौंके। दूर से दो जीपों की बत्तियाँ चमकती नजर आईं। यह क्या? यह तो तय नहीं हुआ था! तस्कर के लोग तो मोटर सायकिलों से आनेवाले थे! ये जीपें कैसी? बात समझने में पटेल बा को क्षण भी नहीं लगा। निश्चय ही किसी भेदिये ने पुलिस को खबर कर दी होगी। अब क्या किया जाए? जीपों की घरघराहट और उनकी रोशनी पल-पल बढ़ती जा रही थी। गाँव से उनकी दूरी हर साँस पर कम होती जा रही थी। छापा कामयाब हो गया तो आधे से ज्यादा गाँव पकड़ा जाएगा! क्या किया जाए?
जैसे किसी आत्मा ने पटेल बा पर अपनी सवारी उतार दी हो इस तरह पटेल बा ने जोर-जोर से चिल्लाना, आवाजें लगाना शुरु कर दिया - ‘डरना मत रे! घबराना मत रे! ये डाकू नहीं हैं। ये तो अपने पुलिसवाले हैं।’ छोटा सा गाँव और कवेलू की छतें। पटेल बा की आवाज गाँव के हर घर में गूँज उठी। जिनकी अफीम थी वे तो पहले से ही अधजगे थे। वे तो पूरे जागे ही जागे, बाकी गाँव भी जाग गया और पटेल बा का मकान मानो पंचायत घर में बदल गया। जिनका ‘माल’ था, वे चीतों की तरह झपटे। अपना-अपना ‘माल’ कब्जे किया। ठिकाने लगा कर वापस पटेल बा के घर पहुँच, भीड़ में शामिल हो गए।
कुछ ही मिनिटों में पुलिस दल पहुँच गया। पूरे गाँव को जमा देख दरोगाजी भन्ना गए। सारा खेल खराब हो चुका था। समझ तो गए थे किन्तु कहते और करते भी क्या? पटेल बा को खरी-खोटी सुनाने लगे। उधर दरोगाजी बिफरे जा रहे इधर पटेल बा मासूम, दयनीय मुद्रा में सफाई दिए जा रहे - ‘क्या गलत किया सा‘ब? डाकू समझ कर गाँव के लोग बन्दूकें चला देते। पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मैंने तो आपको और गाँववालों को बचाया सा‘ब! और आप हैं कि मुझे डपटे जा रहे हैं! सच्ची में भलमनसाहत का तो जमाना ही नहीं रहा।’ पूरा गाँव पटेल बा की हाँ में हाँ मिलाता, मुण्डियाँ हिला रहा। दरोगाजी की झल्लाहट देखते ही बनती थी।
दरोगाजी आखिर कब तक चिल्लाते? जल्दी ही चुप हो गए। पटेल बा ने गाँववालों को डाँटा - ‘अपना आराम छोड़ कर आधी रात को हाकम आए हैं। तुम आँखें फाड़े देख रहे हो! कुछ तो शरम करो! गाँव का नाम डुबाओगे क्या? हाकम को कम से कम पानी की तो पूछो!’ सुनते ही पूरा गाँव ताबेदारी में जुट गया। फटाफट देसी घी का हलवा बनाया और लोटे भर-भर ‘कड़क-मीठी’ चाय पेश की।
भुनभुनाते हुए दरोगाजी चलने को हुए तो पटेल बा ने कुछ इस तरह मानो मक्खन में छुरी गिर रही हो, ‘मालवी मनुहार’ की - ‘सा’ब! अब आधी रात में कहाँ जाओगे? गाँववालों के भाग से आपका आना हुआ। रात मुकाम यहीं करो। सवेरे कलेवा करके जाना।’ दरोगाजी तिलमिला उठे। मानो कनखजूरे पर चीनी छिड़क दी हो। चिहुँक कर बोले - ‘रहने दो पटेल! रहने दो। मुँह में आया निवाला तो आधी रात को छीन लिया और सुबह के कलेवे की मनुहार कर रहे हो। तुम्हारी मनुहार का मान फिर कभी रखूँगा। याद रखूँगा और राह देखूँगा। लेकिन तुम भी याद रखना। जब कभी मेरे ठिकाने पर आओगे तो कलेवा तो क्या पूरा भोजन कराऊँगा। वो भी बिना मनुहार के।’
बमुश्किल अपनी हँसी रोकते हुए पटेल बा, नतनयन, दीन-भाव से विनीत मुद्रा में बोले - ‘आप हाकम, हम रियाया। जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे हजूर। आप नाराज हों, आपकी मर्जी। अपने जानते तो हमने कोई गुनाह नहीं किया। फिर भी आप सजा देंगे तो भुगत लेंगे हजूर! ग्रीब तो जगत की जोरू होता है। भला हाकम से हुज्जत कर सकता है?’
ठठाकर हँसते हुए पटेल बा ने कहा - ‘आग उगलती आँखों से देखते हुए दरोगाजी ने बिदा ली। उनकी जीपों ने गाँव छोड़ा भी नहीं कि मेरे घर के सामने जश्न मनने लगा। लोगों ने मुझे कन्धों पर उठा लिया। उसके बाद किसी ने गाँव का पटेल बनने की बात सोचना ही बन्द कर दी। नया पटेल तभी बना जब मैंने अपनी मर्जी से पटलई छोड़ी।’
मैंने पूछा - ‘वो सब तो ठीक है लेकिन आपको भोजन कराने की, दरोगाजी की हसरत पूरी होने का मौका तो नहीं आया?’ पटेल बा बोले - ‘दरोगा गुस्सैल जरूर था लेकिन मूरख नहीं। अपनी आँखों देख लिया था कि पूरा गाँव मेरी पीठ पर है। कुछ ही दिनों बाद उसने खुद ही दोस्ती कर ली।’ मैंने शरारतन पूछा - ‘आपके हर काम से दोस्ती कर ली?’ जोरदार धौल टिकाते हुए बोले - ‘पोते का दादा हो गया लेकिन अब तक अक्कल नहीं आई। उस दिन क्या उस बेचारे की फजीहत कोई कम हुई जो आज तू फिर मुझसे उसकी फजीहत कराना चाहता है।?’
ठठाकर हँसते हुए, पटेल बा ने मुझे बाँहों में भर लिया।
-----