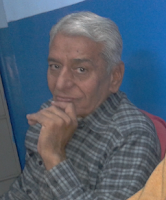अदम्य : जन्म शाम 7.04 पर। यह चित्र 7.55.41 बजे का।
इससे मिलिए। यह है ‘अदम्य’ - हमारी मौजूदा गृहस्थी की तीसरी पीढ़ी का पहला सदस्य। हमारा पहला पोता। इसका जन्म तो हुआ 22 मार्च की शाम 7 बजकर 4 मिनिट पर पर। किन्तु उस सुबह 5 बजे से ही हमारी सम्पूर्ण चेतना, सारी गतिविधियाँ, सारी चिन्ताएँ, सारे विचार इसी पर केन्द्रित हो गए थे - इसकी माँ, प्रशा को उसी समय इसने अपने आगमन की पहली सूचना दी थी।
21 मार्च की शाम को, प्रशा को, डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने कहा था - 15 अप्रेल को या उसके बाद ही प्रसव होगा। किन्तु 21 और 22 मार्च की सेतु रात्रि में, कोई दो बजे से प्रशा असामान्य हो गई। कोई तीन घण्टे तक वह सहन करती रही। अन्ततः, सुबह पाँच बजे अपनी सास, मेरी उत्तमार्द्ध को उठा कर अपनी स्थिति बताई। उन्होंने मुझे उठाया और फौरन ही डॉक्टर से फोन पर बात की। डॉक्टर ने कहा - ‘स्नान-ध्यान कर आठ बजे ले आइए।’
सुबह 8 बजे प्रशा को अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने पहले ही क्षण कहा - ‘डिलीवरी आज ही होगी। शाम चार बजे तक नार्मल की प्रतीक्षा करेंगे। नहीं हुआ तो सीजेरियन करना पड़ेगा।’
परिवार में हम दो ही सदस्य और दोनों ही अस्पताल में। याने हमारा पूरा परिवार अस्पताल में। सुबह नौ बजे बेटे वल्कल को, मुम्बई सूचित किया। शाम छः बजे वल्कल पहुँच गया। मुम्बई से इन्दौर तक वायुयान से और इन्दौर से रतलाम तक मोटर सायकिल से यात्रा की उसने।
चार बजे तक तो हम सब सामान्य थे किन्तु उसके बाद से, ‘सीजेरियन’ की कल्पना से ही घबराहट होने लगी। प्रशा को चार बजे से ही डाक्टर और नर्सों ने ‘लेबर रूम’ में ले लिया था। उनकी भाग-दौड़ हमें नजर तो आ रही थी किन्तु कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा था। घड़ी के काँटे जैसे-जैसे सरकते जा रहे थे, मेरी आँखों के आगे चाकू-छुरे नाचने लगे थे। अस्पताल के कर्मचारियो में से कोई भी हमसे कुछ नहीं कह रहा था किन्तु मुझे बार-बार ‘आपमें से कौन खून दे रहा है?’ सुनाई दे रहा था। मेरी नसें खून का दबाव नहीं झेल पा रही थीं। मैं अपनी ही धड़कनें साफ-साफ सुन रहा था। मेरी कनपटियाँ चटक रहीं थीं। घबराहट के मारे मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहा था - प्रशा को सीजेरियन से बचा ले।
पाँच बज गए। छः बज गए। नर्सों की आवाजाही कम हो गई थी। सात बज गए। लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं। मैं पस्तहाल हो, ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पर बैठ गया। लगभग सात बजकर दस मिनिट पर एक नर्स बाहर आई और मेरी उत्तमार्द्ध से बोली - ‘आप कुछ कपड़े लाए या नहीं? लाइए! कपड़े दीजिए।’ मेरी उत्तमार्द्ध पूरी तैयारी से आई थी। फौरन ही कपड़े दिए। कपड़े लेकर नर्स जिस तरह से अचानक प्रकट हुई थी, उसी तरह अन्तर्ध्यान हो गई। न तो उसने बताया और न ही उसने पूछने का मौका दिया कि कपड़े माँगने का मतलब क्या है। मैं ही नहीं, हम सब सकते में थे। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी, मेरी बाँह थपथपाकर, ढाढस बँधाते हुए मेरी उत्तमार्द्ध बोलीं - ‘खुश हो जाइए। डिलीवरी हो गई है। आप दादा बन गए हैं।’ मुझे विश्वास नहीं हुआ। नर्स ने तो कुछ नहीं कहा! फिर ये कैसे कह रही हैं? मैंने पूछा - ‘आपको कैसे मालूम? नर्स ने तो कुछ भी नहीं कहा।’ वे सस्मित बोलीं - ‘ईश्वर ने यह छठवीं इन्द्री हम औरतों को ही दी है। कुछ पूछिए मत। किसी को फोन कीजिए। फौरन मिठाई मँगवाइए।’ मैं नहीं माना। मैं कुछ पूछता उससे पहले नर्स फिर प्रकट हुई। मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही वह, हवाइयाँ उड़ती मेरी शकल देख, मुस्कुराती हुई मेरी उत्तमार्द्ध से बोली - ‘सर को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। डिलीवरी हो गई है। नार्मल हुई है और बाबा हुआ है।’ कह कर नर्स एक बार फिर हवा हो गई।
ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हम तमाम लोग एक क्षण तो कुछ भी समझ नहीं पाए। लेकिन पलक झपकते सब समझदार हो गए। सब हमें और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन हम दोनों? पता नहीं क्या हुआ कि ‘डिलीवरी नार्मल हुई है’ सुनकर हम दोनों के हाथ अपने आप ही आकाश की ओर उठ गए। हम दोनों की आँखें झर-झर बह रहीं थीं। उस क्षण हमें भले ही अपना भान नहीं था किन्तु हमें, अपनी वंश बेल बढ़ने से अधिक प्रसन्नता इस बात की थी कि हमारी प्रशा, सीजेरियन का आजीवन कष्ट भोगने से बच गई। ईश्वर की यह अतिरिक्त कृपा हमें अनायास ही ‘उसके प्रति’ नतमस्तक किए दे रही थी। हमें सामान्य होने में तनिक देर लगी और जब हम खुद में लौटे तो रोमांचित थे - ‘अरे! हम तो दादा-दादी बन गए!’ हम दोनों आपस में कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। थोड़े सहज हुए तो हम दोनों ने वल्कल को बधाइयाँ और आशीष दी। तभी नर्स, हमारे परिवार की अगली पीढ़ी के पहले सदस्य को कपड़ों में लिपटाए लाई और मेरी उत्तमार्द्ध को थमा दिया। उपस्थित लोगों के मोबाइल की फ्लेश गनें चमकने लगीं।
इसके बाद जो-जो होना था, वह सब हुआ। हमारी जिन्दगी बदल चुकी थी। क्या अजीब बात है कि एक नवजात शिशु ने पल भर में हमें बूढ़ा बना दिया था और हम थे कि निहाल हुए जा रहे थे!
फुरसत में तो हम पहले भी नहीं थे किन्तु इस शिशु ने हमें अत्यधिक व्यस्त कर दिया। हमारी व्यस्तता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 22 मार्च के बाद मैं अब यह पोस्ट लिख पा रहा हूँ - कोई डेड़ माह बाद। ये तीन पखवाड़े हम लोग जिन्दगी भर नहीं भूल पाएँगे।
22 मार्च को पोता आया और 30 मार्च को मेरी जन्म तारीख थी। दोनों प्रसंगों पर हमारे परिवार पर और मुझ पर, कृपालुओं/शुभ-चिन्तकों की जो अटाटूट कृपा-वर्षा हुई, उस सबके प्रति मैं धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करने का न्यूनतम, सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभा पाया।
मेरी इस पोस्ट को ही मेरा धन्यवाद/कृतज्ञता ज्ञापन और मेरी क्षमा याचना मानें, स्वीकार करें और उदारमना हो, मुझे क्षमा करने का उपकार करें।
इन तीन पखवाड़ों के हमारे अनुभव आपको निश्चय ही आनन्द देंगे। आप सब हमारे मजे ले सकें, इसलिए वह सब लिखूँगा - जल्दी से जल्दी।
पोते को निहारती दादी: चित्र 7.45.39 बजे।
अपने बेटे के साथ मुदित मन माता-पिता, प्रशा और वल्कल। चित्र 7.51.04 बजे।
अपने नवजात बेटे को देख खुश हो रहा पिता, वल्कल। चित्र 7.55.11 बजे।
.jpg)